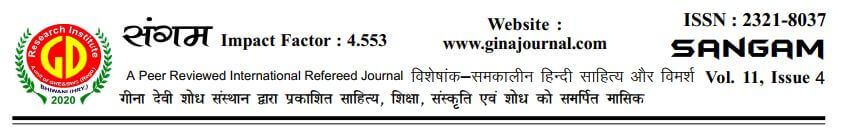40. समकालीन हिन्दी साहित्य में दलित विमर्श – सोमबीर
Page No.:276-284
समकालीन हिन्दी साहित्य में दलित विमर्श – सोमबीर
शोध आलेख सार
दलित साहित्य आज एक ऐसा विषय बन चुका जिसका अध्ययन किये बिना सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य को समझना अनुचित हैं। इस दिशा में अधिक मात्रा में लेखन होना दर्शाता है. कि यहाँ पर भी चेतना कम नही है। दलित साहित्य का मुख्य उदेश्य समाज मंे दलित जीवन की आधारभूत समस्याओं ंके बारे में जनता को बताना है। अभी तक इस बात में संदेह है कि दलित साहित्य के लेखन में किसको शामिल किया जाऐ। दलित साहित्यकारों का कहना है कि दलित की पीड़ाओं को वही समझ सकता जिसने इनको भोगा है। विख्यात दलित चिन्तक कँवंल भारती लिखते हैं, ‘‘दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें स्वंय दलितों ने अपनी पीड़ा को रूपायित किया, अपने जीवन संघर्ष में जिस संघर्ष को भोगा है, दलित साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नही बल्कि जीवन का और जीवन की जीजिविषा का साहित्य है। दलित साहित्य साहित्य सातवीं शताब्दी की एक विधा के रूप में उभरा और आज दलित साहित्य की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। आरंभिक दौर में ज्यादातर कविताएं ही लिखी गई। सातवें दशक में दलित साहित्यकारों ने कहानी विधा को अपनाया उस समय इन कहानियों को संपादको द्वारा ज्यादा महत्व नही दिया गया लेकिन फिर भी दलित रचनाकार कहानियाँ लिखतें रहें। दलित रचनाकारों ने अपने हौसले को नही छोड़ा। दलित कहानियों का समकालीन परिदृश्य आठवे दशक में तेजी से उभरता हुआ दिखाई देता हैं। हिंदी कहानी में नई कहानी, अकहानी, समान्तर कहानी तथा जनवादी कहानी आदि पड़ाव से गुजरते हुए हिंदी कहानी का रुझान उसे वैचारिक प्रतिबद्धता से जोड़ता है। आधुनिक काल में साहित्यकारों ने जातिगत रूढ़ियो के मूलोच्छेद के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उत्तर आधुनिक युग में दलितों में अस्तित्व बोध की पीड़ा को लेकर प्रस्फुटित स्फुलिंग दहकता अंगारा बन जड़ व्यवस्था को दग्ध करने को मचल उठा। दलित साहित्यकारों में मोहनदास नैमिशराय, सूरज पाल चौहान, ओमप्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले, जयप्रकाश कर्दम, ग्योराज सिंह बेचैन, रजतरानी, सुदेश तनवीर ने साहित्य की विविध विधाओं में शोषण और अपमान की प्रतिक्रिया की दर्द भरी और रोषपूर्ण अभिव्यक्ति की। दलित पत्रिकाओं (दशंबूक, युद्धरत, आम आदमी) का प्रकाशन हुआ। दलित चेतना के आधार पर हिंदी साहित्य का पुनर्पाठ किया गया और 1914 में सरस्वती – में प्रकाशित हीरा डोम की कविता ’अछूत की शिकायत‘ को हिन्दी की प्रथम दलित रचना के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। आज दलित साहित्यकार परम्परागत काव्यशास्त्र और सौन्दर्य बोध के स्थान पर साहित्य की नवीन कसौटी की खोज कर रहे है तथा अफ्रीका की अश्वेत जातियों के साहित्य से प्रेरणा प्राप्त कर रहे है। इन साहित्यकारों ने काव्यशास्त्रीय मान्यताओ को नकारा है तथा अन्याय का विरोध करने के कारण इनकी भाषा चुटीली एवं व्यंग्यात्मक है। इस साहित्य के द्वारा दलित अस्मिता को सफलता पूर्वक रेखांकित किया गया है, किन्तु यदि जातिवादी क्रोध, प्रतिहिंसा एवं घृणा के रूप में सामने आती है, तो चिन्तनीय है।
मुख्य शब्द: साहित्य, दलित साहित्य, शोषण, संघर्ष।
प्रस्तावना:
दलित शब्द का अर्थ है- दबाया गया, कुचला गया, उत्पीड़ित। पहले जब भारतीय समाज चार वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णो की व्यवस्था कर्मानुसार की गई थी। शूद्र वर्ण जो कि सबसे निचले पायदान पर था, शताब्दियों से शोषण, दमन व असमानता का शिकार हो रहा था तथा उच्च वर्ण द्वारा इस वर्ण का अनेक प्रकार से उत्पीड़न कर रहा था। इस वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार न रहकर जन्मानुसार, हो गई तो इस वर्ण के लोगो को शिक्षा व समानता आदि अधिकारों से वंचित रखा गया। समय बीतने के साथ-साथ इनकी अस्मिता विलीन हो गई।
आधुनिक काल में अनेक समाज सुधारकों का ध्यान इन लोगो पर गया। उन्होने इस समाज को अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयत्न किये। इस संदर्भ में एक और तो अस्पृश्यता व वर्णगत असमानता को दूर, करने के लिए राजा राम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी आदि विभूतियों ने समाज सुधार के प्रयत्न किये तो दूसरी और ज्योति बा फूले, नारायण गुरू तथा भीमराव अम्बेडकर जैसे दलित वर्ग की विभूतियों ने ’परिवर्तन’ का स्वर बुलन्द किया।
दलित विमर्श का आरंभ मराठी साहित्य से हुआ उसके बाद हिन्दी, गुजराती, कन्नड, मलयालम, तेलगु, व तमिल में भी दलित साहित्यकारों द्वारा रचित साहित्य के स्वर सुनाई देने लगे। हिन्दी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन दास नैमिषराय, डॉ० ए० एन० सिंह कँवल भारती, डॉ0 धर्मबीर प्रभृति अनेक दलित साहित्यकारों ने दलित साहित्य की विशेष स्थिति और आवश्यकताओ को रेखांकित करते हुए प्रतिपादित किया।
दलित कहानी समाज के फैली विसंगतियों और अराजकता को ख़त्म करने का मार्ग भी खोजती है। अम्बेडकर दलित साहित्य के आधार हैं उनकी विचारधारा ही दलित कहानियों का प्राण तत्व है। उनका साहित्य और सम्पूर्ण लेखन दलित जीवन को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए लिखा गया है। वह जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे तथा उसके नाम पर फैलाये जा रहे सांप्रदायिक परिवेश के भी खि़लाफ़ थे। उनका मानना था- “जाति ने हालाँकि एक काम किया है। इसने हिन्दू समाज को पूरी तरह से असंगठित और अनैतिक अवस्था में ला दिया है। …यह तो जातियों का समूह मात्र है। प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व के प्रति सचेत है। इनका अस्तित्व जाति-व्यवस्था के जारी रहने का कुल परिणाम है। जातियाँ एक संघ भी नहीं बनातीं। कोई जाति दूसरी जातियों से जुड़ने की भी भावना नहीं रखती, सिर्फ़ हिन्दू-मुस्लिम दंगे के समय ये आपस में जुड़ती हैं।”
दलित कहानियाँ दलित जीवन में जबरन भर दिये गए अपमान और तिरस्कार के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं साथ ही दलित समाज की अपनी विसंगतियों को भी अभिव्यक्त करती हैं। दलित साहित्यकारों ने अपने समाज में फैले आडंबर और सामंतवादी मानसिकता को भी ख़त्म करने का आह्वान किया है- “दलित समाज को अपनी मुक्ति के लिए सवर्णों से ही नहीं अपितु स्वयं से ही भी संघर्ष करना पड़ेगा। यह बहुत पीड़ा दायक और मुक्ति की राह में बड़ी रुकावट है।”
जितने भी दलित साहित्यकारों ने समाज और साहित्य में अपना सम्मानित स्थान बनाया है, सभी ने शिक्षा के बल पर यह स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा दलित समाज की बुनियाद को मज़बूत करती है। दलित साहित्यकारों ने यह प्रेरणा भी बाबा साहब से ली है। आंबेडकर दलितों को शिक्षित करनेके सभी प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध से सरकारी, ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के साथ अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा वह उन्हें शिक्षित करना चाहते थे। शिक्षा द्वारा ही दलितों और स्त्रियों में अपने अधिकार और अस्मिता को समझने की चेतना आयी। डाली शिक्षा द्वारा ही स्वयं के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए एकत्र हुए। आंबेडकर कहते थे- ‘शिक्षित बनो’, ‘संगठित हो’ और ‘संघर्ष करो’ एवं ‘अप्पो दीपो भव’ अर्थात् ‘अपना दीपक स्वयं बनो’! बाबा साहब के इन्हीं शब्दों ने सदियों से शोषित दलितों के अंदर सोयी हुई उदासीनता को तोड़कर उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। आंबेडकर का मानना था कि “प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति में अपनी रक्षा की क्षमता होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी भी है।”
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद दलितों के मन में यह आशा आकांक्षा थी कि अब रूढ़िवादी परंपरा का अंत होगा छुआछूत की भावना से हम मुक्त होंगे। संविधान के अनुसार शिक्षा तथा नौकरियाँ में हमें आरक्षण मिलेगा कुछ हद तक दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है। दलित शिक्षित होने लगे, नौकरियां मिलने लगी, किन्तु समानता नहीं मिली। भेद-भाव की भावना आज भी हमें दिखाई देती है। इसीलिए तो दलित साहित्य का सृजन अन्य साहित्य की तुलना में ज्यादा जोर पकड़े हुए है। सूरजपाल चैहान की ’साजिश’ कहानी का नत्थू कठिनाई से बी. ए. की परीक्षा पास करके ट्रान्सपोर्ट के धन्धे के लिए बैंक से कर्जा लेना चाहता है, किन्तु बैंक मैनेजर रामसहाय शर्मा, नत्थू की दिशाभूल करके उसे सूअर पालने के लिए कर्ज देना इसीलिए पसंद करता है, क्योंकि नत्थु एक अछतू वर्ग का युवक है। मैनेजर शर्मा अपने हेडक्लर्क सतीश भरद्वाज से कहता है, “देख सतीश अगर ये अछूत अपना खानदानी धन्धा बन्द कर कोई नया धन्धा करने लगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे घरों की गन्दगी कैसे साफ करेगी। उस स्थिति में घर की गन्दगी क्या तुम खुद साफ करोगे?
दलित साहित्य भोगे हुए यथार्थ का धघकता हुआ प्रामाणिक दस्तावेज है। वह अनुभव की आँच पर तपकर निकला हुआ सत्य है। दलित साहित्य में दलितों के तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं के भोगे हुये यथार्थ के आधार पर प्रामाणिक एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है। दलितों का मानना है कि उनका उत्थान केवल संघर्ष के द्वारा होगा। कहीं-कहीं दलित साहित्य दलित राजनीति से प्रभावित जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में दलित साहित्य का उद्देश्य उत्तर आधुनिक विमर्श के स्थान पर उत्तर हिन्दू विमर्श के रूप में दिखायी देता है। फलस्वरूप असन्तोष एवं आक्रोश की परिणति अजातिवादी क्रोध, प्रतिहिंसा और घृणा के रूप में भी सामने आयी है, जो निश्चित रूप से चिन्तनीय है, किन्तु अब देखा जा रहा है कि दलित साहित्य भी सहजता की ओर बढ़ रहा है। हिन्दी में दलित लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि का कथा साहित्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वे दलित समुदाय की पीड़ा और आक्रोश का बेबाक चित्रण करते हैं लेकिन उसकी आड़ में किसी ’दलित धर्म’ या ’दलितवाद’ का प्रस्ताव नहीं करते। दलित समुदाय के भीतर उनकी परम्पराओं को आलोचक की दृष्टि से देखते है और जहाँ आवश्यक होता है. उसकी खामियों की ओर उँगली उठाते हैं। ’हत्यारे’ कहानी में उन्होनें दलितों में व्याप्त अन्धविश्वास को बखूबी रेखांकित किया है। अस्मितावाद से शुरू कर सार्वभौम मनुष्यता तक पहुँचना उनका गन्तव्य है। ’सलाम’, ’खानाबदोश’. ब्रह्मास्त्र’ कहानियों में द्विज पात्र दलितों का साथ देना चाहते हैं लेकिन आधी दूर चलकर ठहर जाते हैं। अभी उन्हें वैचारिक व भावात्मक रूप से पुख्ता होने में समय लगेगा। ’घुसपैठिया’ कहानी में लेखक ने मेडिकल कॉलेज में दलित छात्र की दशा को रेखांकित किया है जहाँ वह शोषण के कारण आत्महत्या कर लेता है, जिसे लेखक हत्या के रूप में देखता है। इनकी कहानियों में दलित पात्रों में हीनता बोध गहराई से पैठा हुआ है, वे कई बार जाति छुपाकर जीवन यापन करते हैं। “मैं ब्राह्मण नहीं हूँ’ का मोहनलाल शर्मा अपनी जाति छुपाकर रह रहा है उसके बेटे की शादी गुलजारी लाल शर्मा की बेटी से तय हो चुकी है। इसी बीच मोहन लाल की बहन मय साजोसमान के आकर भेद खोल देती है कि वह शर्मा नहीं मिरासी है। गुलजारी लाल को मौका मिलता है वे मोहनलाल को जी भरकर जलील करते हैं लेकिन उनकी खुद की असलियत यह है कि वे बढ़ई से ब्राह्मण बने हैं। इन दोनों परिवारों की नयी पीढ़ी इन पाखण्डों से मुक्त होना चाहती है। ’दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन’ कहानी भी जाति-गोपन की कोशिशों के इर्द-गिर्द बुनी गयी है। ’कूड़ाघर’ कहानी में अजब सिंह का परिवार किराये के मकान से इसलिये बेदखल कर दिया जाता है, क्योंकि मकान मालिक को उसकी जाति का पता चल जाता है। ’प्रमोशन’ कहानी में मजदूर संगठनों के बीच पसरे जातिवाद का खुलासा किया है। सुरेश स्वीपर से प्रमोद होकर मजदूर बन जाता है। वह ’लाल झण्डा यूनियन का मेम्बर बनकर उसकी गतिविधियों में जोर-शोर से शामिल होता है। वह कामरेड सम्बोधन से रोमांचित होता है। मजदूर मजदूर भाई के नारे का अर्थ उसे तब समझ में आता है जब उसके हाथ से बँटने वाले दूध को कोई लेने नहीं पहुँचता है। लोगों की नजर में वह आज भी स्वीपर है। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि दलितों में भी परस्पर ऊँच-नीच की भावना व्याप्त है। अन्य दलित भंगी को अस्पृश्य मानते हैं, यह विडम्बना है।
भारत में दलित साहित्य की गूँज छठे दशक से सुनाई देने लगी। दलित स्वर अब समस्त समाज को अपनी वाणी से परिचालित और उद्वेलित कर रहा है। आज़ादी के पश्चात् नया संविधन 1950 में लागू हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग और वर्ण से परे समतामूलक समाज के निर्माण और सामाजिक न्याय तक प्रत्येक भारतीय की पहुँच की आकांक्षा के साथ दलितों के मसीहा डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में नए भारत के लिए नए संविधान का निर्माण और इसके साथ ही एक नए युग का सूत्रपात हुआ। देखा जाए तो बीसवीं सदी के पूर्वोत्तर में भारतीय राजनीति के मंच पर सक्रिय भूमिका में डॉ. आम्बेडकर ने पहली बार समाज के एक बड़े हिस्से की लड़ाई की शुरुआत की जो दलित था, शूद्र था, अस्पृश्य था, दास की भूमिका में अमानवीय स्थितियों में जीने के लिए अभिशापित था। सामाजिक स्तर पर पूरे दलित समाज को पहली बार डॉ. आम्बेडकर ने उद्वेलित किया और उसे आंदोलनकारी भूमिका प्रदान की। बाबा साहेब ने नारा दिया था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो- इस बोध वाक्य को दलित समाज ने अपने जीवन का मूलमंत्र बना लिया; संपूर्ण दलित साहित्य अपनी वैचारिक ऊर्जा अम्बेडकर से ही ग्रहण करता है। दलित साहित्य के समस्त विधाओं में दलितों की व्यथा कथा और अनुभवों का यथार्थ चित्रण है।
आक्रोश और नकार दलित साहित्य के दो मुख्य मुद्दे है। सम्पूर्ण भारतीय दलित समाज की स्थिति एक जैसी है। उनके दुःख, संताप एक जैसे हैं और यही कारण है कि दलित लेखन भी अभिव्यक्ति के स्तर पर एक जैसा ही है। दलित लेखन को अगर देखा जाय तो इस क्षेत्र में काव्य सृजन अधिक हुआ है। कविताओं में, पीड़ा में डूबी भावनाओं और विरोध के रूप में प्रहारात्मक तर्क ने जनमानस को बहुत प्रभावित किया । गौरतलब है कि समस्त भारतीय कविता का मूल स्वर वर्णव्यवस्था से पीड़ित समुदाय की वेदना है, जिसकी जड़ में सदियों से सामाजिक न्याय से वंचित, अत्याचार और शोषण का इतिहास है। भारतीय दलित कविता वर्ण व्यवस्था की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक वर्चस्व के खि़लाफ़ एक मोर्चा है। यह यातनाओं के अतीत के साथ समसामयिक जीवन और परिवेश से जुड़ने के कारण प्रासंगिक है – या यों कहें कि इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, नकार और विद्रोही स्वर के साथ-साथ परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा को भी वाणी दे रही है।
यूँ तो कविता का इतिहास वर्षों पुराना है। विविध छंदों से होती हुई छंद मुक्त हुई कविता के कई रंग देखे जा सकते हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हिन्दी कविता ने कई रंग बिखेरे हैं। साहित्य और समाज का संबंध मनुष्यता के विस्तार के लिए हुआ है। साहित्य शब्द का प्रचलन सातवीं-आठवीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। साहित्य का आरंभ “कविता” से हुआ। आरंभिक समय भारतीय साहित्य में कविता ही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। साहित्यिक विधा के रूप में अन्य विधाओं का आगमन अभी नहीं हुआ था लिहाजा काव्य रूप को ही साहित्य माना गया। संस्कृत में साहित्य के स्थान पर ‘काव्य’ शब्द का प्रयोग मिलता है। उस समय के विख्यात आचार्यों ने साहित्य को अपनी मान्यता के अनुसार व्याख्यायित करने का प्रयास किया। भामह, राजशेखर, कुंतक आदि आचार्यों ने काव्य की परिभाषा देते हुए शब्द और अर्थ के तमाम पक्षों पर विचार किया, जिसमें शब्द और अर्थ का सहभाव ही ‘काव्य’ अथवा ‘साहित्य’ माना। कुछ समय बाद आपसी स्वीकृति और समझौते के बाद संस्कृत में भी साहित्य शब्द का प्रयोग होने लगा। आगे चलकर ‘काव्य’ शब्द ‘साहित्य’ शब्द के अर्थ में रूढ़ हो गया। आधुनिक काल में कविता ही मात्र अभिव्यक्ति का साधन नहीं रह गयी। साहित्यकारों और चिंतकों ने लेखन को आम जनता तक ले जाने के उद्देश्य से उसे विस्तारित और सरल किया। विस्तार की इसी प्रक्रिया में तमाम अन्य विधाओं का भी जन्म हुआ जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध के साथ समीक्षा और आलोचना का भी विकास हुआ। इन तमाम विधाओं को ‘साहित्य’ कहने से कोई अवरोध नहीं दिखता। बल्कि कविता को साहित्य कहने से सीमित अर्थ की ध्वनि उत्पन्न होती है। साहित्य अन्य कलाओं से से अलग समाज से संबंध बनाने में अधिक प्रभावशाली है। समाज और साहित्य के बीच भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना भाषा इस संबंध की कल्पना ही संभव नहीं है। जिस भाषा को प्रयोग करने वालों की संख्या जितनी कम होगी उसका साहित्य उतना ही कमज़ोर और सीमित होगा। आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने साहित्य और समाज के संबंध को इन शब्दों में व्यक्त किया है- “साहित्य और जीवन का क्या संबंध है, यह प्रश्न है आज एक विशेष प्रयोजन से पूछा जाता है। वर्तमान भारतीय समाज एक ऐसी अवस्था पर पहुँच गया है जिसके आगे अज्ञात संभावनाएँ छिपी हुई हैं। विशेषतः हमारे शिक्षित नवयुवकों के लिए यह क्रांति की घड़ी है।” महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ते हुए कहते हैं- “जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है, उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति के जीवन शक्ति इस समय कितनी या कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी।‘‘
भारतीय समाज और साहित्य का गहरा सम्बन्ध हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक है। साहित्य समाज आत्मा साहित्य है। साहित्य मानव मस्तिष्क से उत्पन्न होता है और मस्तिष्क वही ग्रहण करता है जो समाज से उसे प्राप्त होता है। साहित्य मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है। मनुष्य न तो समाज से अलग हो सकता है और न साहित्य से। मनुष्य का पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा तथा जीवन निर्वहन भी समाज में ही होता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनकर अनेक अनुभव ग्रहण करता है, जब वह इन अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है तो साहित्य का रूप बन जाता है। शब्दों की यही अभिव्यक्ति आदमी को श्रेष्ठ एवं साहित्यकार बना देती है। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व-बन्धुत्व के सदभाव के साथ हाशिये के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्यकार समाज और अपने युग की को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता है क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज के अस्मिता की पहचान होता है। भारत की आज़ादी के संग्राम के समय भारतीय समाज और साहित्य का पता दुनिया को हो चुका है। अंग्रेज़ों को देश छोड़कर भागना पड़ा, इसमें भारतीय समाज और साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही। साहित्य मानव जीवन को परिवर्तन के साथ अन्य मानवजाति को जोड़ता भी है इसीलिये हमारे समाज में साहित्य, समाज का प्रतिबिम्ब माना जाता है। साहित्य बीते हुये कल का आईना है और भविष्य के जीवन को दिशा देने वाला भी है। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता साहित्य जीवन के मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है। वाल्मीकि, कालीदास, रविदास, सूरदास, तुलसीदास एवं आधुनिक युग के साहित्यकारों की रचनाएँ आज के पूँजीवादी और व्यावसायिक युग में भी आधुनिक समाज का दिशा निर्देशन करने में सक्षम हैं।
संदर्भ ग्रन्थ
सोमबीर
नेट, जे॰ आर॰ एफ॰
हिन्दी विभाग,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)