70.समकालीन हिंदी नाटकों में स्त्री-विमर्श – बी. वी. एन् उमा गायत्री
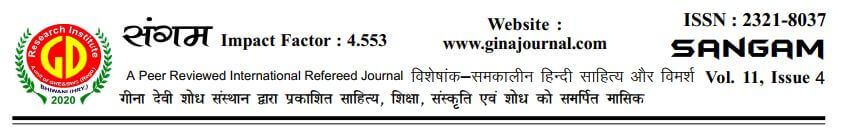 Page No.: 503-509
Page No.: 503-509
समकालीन हिंदी नाटकों में स्त्री-विमर्श
बी. वी. एन् उमा गायत्री
शोध-सार-:
भारत में स्त्री को सदा से ही समाज में एक अनिवार्य स्थान प्राप्त है। यह दूसरी बात है कि वह सम्मान की पात्र रहीं कि नहीं। प्राचीन काल में स्त्री को मात्र एक शरीर के रूप में न देखकर उसे समाज में समान अधिकार व सम्मान प्राप्त था जिसके उदाहरण स्वरूप वैदिक काल की ऋषिणियों को देखा जा सकता है। बाद में धीरे-धीरे अनेक संकुचित विचारों व कुरीतियों से ग्रस्त होते आए हमारे समाज में खोखले मूल्यों व आदर्शों के नाम पर स्त्री के अस्तित्व को मात्र प्रजनन के लिए, पुरुषों के भोग के लिए व उनकी सेवा के लिए ही सीमित करके देखा जाने लगा। किंतु आधुनित सोच व जन-चेतना के चलते अब स्थितियों में परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। बीसवीं शताब्दी से हिंदी के नाट्य-साहित्य में स्त्री चरित्रों की दशा में परिवर्तन व नवीन चेतना दृष्टिगोचर होने लगती हैं। उत्तराधुनिक कालीन समाज व साहित्य में यह परिवर्तन विशेष रूप से प्रखर हो उठता है। पस्तुत शोध-आलेख में कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के आधार पर समकालीन हिंदी नटकों में स्त्री-विमर्श को दर्शाने का प्रयास किय जाएगा।
बीज शब्द-: अस्मितामूलक विमर्श, अस्तित्ववाद, समकालीन साहित्य, पितृसत्ता
प्रस्तावना-:
हिंदी के समकालीन नाट्य-साहित्य में स्त्री-विमर्श पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करना आवश्यक है। सर्वप्रथम ‘समकालीन साहित्य’ शब्द की अवधार्णा को समझने की चेष्टा करे तो हमे यह ज्ञात होता है हि समकालीन शब्द का शाब्दिक अर्थ है वर्तमान काल का या एक ही समय में साथ-साथ घटने वाली घटनाएँ। मगर साहित्य-जगत में आकर इसकी अवधारणा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह एक शब्द मात्र न रहकर एक विशेष प्रवृत्ति से संबद्ध साहित्य का ध्योतक बन जाता है। समकालीनता का संबंध साहित्य में आधुनिक व उत्तराधुनिक प्रवृत्तियों से है। आज के साहित्य में उभरते सभी प्रकार के अस्मितामूलक विमर्श आधुनिक-बोध से युक्त चिंतन परंपराएँ हैं। अतः किसी भी काल की कोई भी ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें आधुनिक- बोध मानसिकता व चिंतन दृष्टीगोचर हो उसे समकालीन साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है।
आज के इस समकालीन-साहित्यिक दौर में अनेक अस्मितामूलक विमर्श अपनी एक विशेष पहचान के साथ सामने उभरकर आ रहे हैं। इन विमर्शों पर आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तरसंरचनावाद, अस्तित्ववाद आदि जैसी कई विचारधाराओं का प्रभाव है जो इन विमर्शों की अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करती हैं। साहित्य-रचना में इन विमर्शों की प्रामुख्यता को समझने के लिए सर्वप्रथम हमे ‘विमर्श’ शब्द के अर्थ और साहित्य में किसी भी विषय को लेकर विमर्श करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। ‘विमर्श’ एक विधिवत चिंतन-प्रक्रिया है और कोई भी अस्मितामूलक विमर्श किसी विशिष्ट वर्ग को उसके अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया जाता है। इनमें सदियों से हमारे समाज में किसी न किसी प्रकार शोषण और दमन का शिकार हुई दलित, आदिवासी, स्त्री, किन्नर, बाल, वृद्ध आदि अनेक तब्के आती हैं जिनके जीवन की अस्मिता और अधिकारों के स्वर को बुलंदी प्रदान करने वाला चिंतन ही साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श कहलाया। इस शोध-आलेख के केंद्र में स्त्री-विमर्श को रखा गया है। चिंतन के स्तर पर देखे तो हमारे साहित्य में हमेशा से तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप स्त्री-अस्मिता संबंधी चिंतन होता रहा है। हालांकि एक विशेष विमर्श के खेमें में बांटकर उसे देखने की प्रवृत्ति साहित्यकारों में समकालीन युग में आई है। अतः आधुनिक काल में खड़ीबोली में नाट्य-रचना के विधिवत आरंभ से ही उसमें स्त्री-विमर्श देखा जा सकता है।
आमुख-:
स्त्री-विमर्श आज के उत्तराधुनिक काल में उभरते हुए अनेक अस्मितामूलक विमर्शों में से एक प्रमुख विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श की यह शाखा एक स्त्री के अस्तित्व को समाज में एक पहचान और उसको उसके मौलिक अधिकार दिलाने का चिंतन-स्वर है। यहां ‘अस्मिता’ और ‘अस्तित्व’ दो शब्द हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में यह दोनों शब्द एक ही अवधारणा के दो छोर हैं। यह दोनों ‘होने के बोध’ की अवधारणा को ही दो विविध आयामों में व्यक्त करते हैं। इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत के ‘अस्’ धातु (होना) से हुई है। ‘अस्’ धातु के लट् लकार (वर्तमान काल) के प्रथम पुरुष का रूप है ‘अस्ति’ जिसका अर्थ है ‘मैं हूँ’ तथा उत्तम पुरुष का रूप है ‘अस्मि’ जिसका अर्थ है ‘वह है’। इन्हीं अवधारणाओं के मूल में समकालीन अस्मितामूलक विमर्श में सहानुभूति और स्वानुभूति के ज्वलंत प्रश्न का भी आधार है और इस प्रश्न का भी समाधान है कि साहित्य में हमेशा से ही कई वर्गों के अस्मितापरक चिंतन के होने के बावजूद इस उत्तराधुनिक काल में ही अस्मितामूलक विमर्श एक विशेष पहचान लेकर क्यों उभरें। वास्तव में पहले साहित्य में किसी वर्ग की अस्मिता और उनके अधिकारों की बात अगर हुई भी है तो वह सहानुभूति के स्तर पर अधिक हुई, आज का स्त्री विमर्श या कोई भी अन्य विमर्श अधिकतर स्वानुभूति को आधार बनाकर चलता है। इसके अतिरिक्त चिंतन के स्तर पर तो कोई काल विभाजन नहीं है क्यों कि साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति रातों-रात नहीं आती या जाती है।
हिंदी साहित्य में आधुनिक काल\गद्यकाल और उसमें खड़ीबोली में नाट्य-साहित्य की शुरुआत भारतेंदू युग से मानी जाती है। तब से ही हिंदी नाटकों में स्त्री-अस्मिता का स्वर प्रख्स्रता से उठया जाता रहा है। इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण नाटकों का उल्लेख यहां किया जा रहा है। भारतेदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक ‘नीलदेवी’ में वे नीलदेवी के माध्यम से धर्मनीति और राजनीति के समन्वय पर बल देते हुए समाज में सदियों से बनी हुई स्त्री की छवि में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। भारतेंदु के बाद हिंदी नाट्य-जगत में प्रमुख नाम जयशंकर प्रसाद का आता है। उन्होंने भी अपने नाटक ‘ध्रुवस्वामिनी’ में स्त्री की स्वाधीनता और स्त्री-अस्मिता के प्रश्नों को उठाया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों द्वारा नारी पर किए जाने वाले शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर प्रखरता से उठाते हुए वे इस नाटक की नाइका से अपने पति द्वार खुद को बेचने की बात जानने पर कहल्वाते हैं कि “मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु-संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते।”[i] दरअसल हमारे समाज में स्वाधीनता आंदोलन और साहित्य में नवजागरण के चलते और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक चिंतन बोध के चलते साहित्य में बहुत सी प्रवृत्तियाँ बदली। इस संदर्भ में जयदेव तनेजा लिखते हैं कि “राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मद्देनज़र भारत में सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों ने महिलाओं को सक्षम बनाया जिससे कि वे समाज और राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय और सार्थक भूमिका निभा सके। इसने साहित्य और नाटक में महिलाओं के चित्यण में कुच बुनियादी बदलाव के लिए नेतृत्व किया।”[ii] इसी क्रम में आज़ादि के बाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक ‘आधे-अधूरे’ भी आता है। इस नाटक में नाटककार मध्यवर्गीय स्त्री-पुरुष संबंधों में बदली सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई विशमताओं और विडंबनाओं की त्रासदी को दर्शाते हुए एक मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन में आर्थिक दबाव और पारिवारिक संबंधों के द्वंद्व में कहीं खो चुकी उसकी अस्मिता की खोज करने का प्रयास करते है।, मणि मधुकर द्वारा रचित नाटक ‘दुलारीबाई’ भी इस बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में स्त्री के अधिकार और उसकी चयन की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाता है। साथ ही यह नारी को परंपरा और संस्कृति के नाम पर दमित करने के लिए इस पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाई गई विवाह-व्यवस्था के खोखलेपन पर भी प्रहार करता है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक ‘शकुंतला की अंगूठी’ भी इस क्रम में उल्लेखनीय है। इसमें नाटककार महाकाव्य ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ की कथा के समानंतर चलती आज की नायिका की कथा बताते हुए यह बताते हैं कि आज की नारि शकुंतला की तरह दुष्यंत (पुरुष-सत्ता) के द्वारा अपना घोर अपमान सहने के बाद भी उसे दूसरा मौका नहीं देती। वह अपने जीवन को चलाना स्वयं जानती है।, प्रभाकर श्रैत्रीय का नाटक ‘सांच कहू तो’ बेमेल विवाहों के चलते नारी-जीवन पर होने वाले अत्याचार को उद्घाटित करता है। इसके पश्चात शंकर शेष का नाटक ‘कोमल गांधार’और भीष्म सहानी का नाटक ‘माधवी’ पौराणिक कथा-वस्तु को आधार बनाकर हमें ठोस यथार्थ के धरातल पर लेजाकर पूरी निर्ममता के साथ समाज में स्त्री-जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। एक तरफ जहाँ ‘कोमल गांधार’ में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार अपने राजनैतिक लाभों के लिए यह पितृसत्तात्मक समाज एक भोली-भाली लडकी को धोखे में रखकर एक अंधे व्यक्ति से उसका विवाह कराता है तो दूसरी तरफ ‘माधवी’ में यह दर्शाया गया है कि एक विवाहित नारी को संतान न होने पर किस तरह अपमानित किया जाता है।
स्त्री नाटककारों में कई ऐसी रचनाकार हुई हैं जिन्होंने स्त्री-विमर्श को आधार बनाकर बहुत ही तीखे व मार्मिक अंदाज़ में नाटक विधा में अपनी कलम चलाई है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय नाटक हैं- नाटककार म्रुदुला गर्ग’ द्वारा रचित ‘एक और अजनबी’ और ‘कितनी कैदें’। इन दोनों नाटकों में नाटककार ने आज के इस उत्तराधुनिक युग के बदलते हुए सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में स्त्री की अस्मिता के प्रश्न को एक नया आयाम प्रदान किया है और उस पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को रेखांकित किया है जो समाज में विद्यमान आधुनिकता के पीछे छिपी हुई रूढीवादी मानसिकता को दर्षाती है। पहले नाटक में उसकी स्त्री पात्र ‘शानी’ की घर तथा बाह्य-जगत दोनों तरफ से उपेक्षाप्राप्त और समस्याओं से ग्रस्त परिस्थितियों को चित्रित किया गया है। एक तरफ वह अपने प्रेमी द्वारा उपेक्षित है तो दूसरी तरफ उसका पति कंपनी में पदोन्नति के लिए अपने मैनेजर के सामने उसको दांव पर लगा देता है। दूसरे नाटलक की स्त्री पात्र ‘मीना’ (मनोज की होने वाली पत्नी) के प्रति ‘मनोज’ का व्यवहार हमारे समाज के पुरुष-वर्ग के दोगलेपन को दर्शाता है। शादी से पूर्व अपनी पत्नी का बलात्कार होने का समाचार पाकर वह प्रतिक्रिया के रूप में कहता है- ‘‘बेवकूफ हो तुम ! इतनी आसानी से अतीत पीछा नहीं छोड़ा करता। … तो जाओ। प्रायश्चित करो। खुदकुशी कर लो। तुम्हारी जैसी औरतें यही करती हैं।“[iii] यह अत्यंत दुःखद व विचारणीय बात है कि आज भी हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाओं में पीड़िता को ही दोशी करार दिया जाता है। इसी प्रकार के विचारों के दोगलेपन तथा ईर्ष्या से ग्रस्त एक पति का चित्रण हमें ‘मन्नू भंडारी’ के नाटक ‘बिना दीवारों के घर’ में भी देखने को मिलता है। नाटक में ‘अजीत’ अपनी पतनी ‘शोभा’ को नौकरी में उन्नति प्राप्त करते देख उसके प्रति ईर्ष्या का अनुभव करने लगता है तथा उसके चरित्र पर संदेह भी करने लगता है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार आधुनिक समाज में पति-पत्नी के ऐसे रिश्ते व उनकी समस्याओं को दर्ज करती हैं जो अपने अहंकार के कारण एक दूसरे के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को फलने-फूलने का अवसर नहीं दे पाते। विशेष रूप से यह स्त्री की स्वतंत्रता के संदर्भ में अधिक देखने को मोलता है।
स्त्रियों के प्रति होने वाले अमानवीय व्यवहार के लगभग सभी आयमों पर हिंदी के साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई है। इसी क्रम में कन्याओं की भ्रूण-हत्या, गर्भ का लिंग-परीक्षण तथा नव-जन्मी शिशु के साथ अमानवीय एवं भेदभाव से युक्त व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए लिखे गए नाटकों में से एक चर्चनीय नाटक हैं- ‘नादिरा ज़हीर बब्बर’ द्वारा रचित ‘जी जैसी आपकी मर्जी’ और ‘सकुबाई’। यह एक दुःखद बात है कि न केवल समाज में अपितु अपने परिवार में भी स्त्रियों को किसी न किसी रूप में दोयम दर्जे का होने का अनुभव कराया जाता है और एक स्त्री की अस्मिता व अधिकारों की लडाई की शुरुआत उसके अपने घर से ही होती है।
इसी क्रम में इतिहास की एक घटना को आधार बनाकर एक पुरुष द्वारा हमेशा अपनी पत्नी को अपने से कमतर ही समझने वाली पुरुषाहंकार की भावना को रेखांकित करता है ‘मीराकांत’ द्वारा रचित ‘कंधे पर बैठा था शाप’। यह महाकवि कालिदास और उनकी उपेक्षित पत्नी विद्योत्तमा की कथा कहता है कि किस प्रकार कालिदास विद्योत्तमा को उनके पाण्डित्य के चलते अपनी गुरु तो मानते हैं मगर उनको अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाते। वह कहते हैं कि “जिस स्त्री ने मेरे जीवन को कीर्ति के शिखर तक पहुंचाया उसे गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में स्वीविकार करना मेरे लिए पाप है।”[iv]
निष्कर्ष-:
इस प्रकार इन सब नाटकों में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के आधार पर और ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति, उसकी अस्मिता और उसके अधिकारों को लेकर विमर्श प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपने प्रति हो रहे अत्याचारों को भली-भांति पहचानती, उसका सामना करने का साहस रखती व पितृसत्ता की कैद से मुक्त स्वतंत्र जीवन जीने का संकल्प रखती आज की नारी के स्वतंत्र अस्तित्व को हिंदी के नाटककारों ने एक दिशा प्रदान करने का कार्य किया है।
[i] ‘ध्रुवस्वामिनी’- जयशंकर प्रसाद, श्री नटराजनटराज प्रकाशन, दिल्ली, सं 20142014, पृष्ठ सं. 33
[ii] ‘हिंदी नाटकों में स्त्री’ (लेख)- जयदेव तनेजा, ‘रंगवार्ता’ पत्रिका, सं. अश्विनी कुमार पंकज, नवंबर-जनवरी 2011-12 अंक, पृष्ठ सं. 54
[iii] ‘कितनी कैदें’- मृदुला गर्ग, 1996, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, पृष्ठ सं. 39-40
[iv] ‘कंधे पर बैठा था शाप’- मीराकांत, 2006, भारतीय ज्ञानपीठ, पृष्ठ. स. 54
शोधार्थी-
बी. वी. एन् उमा गायत्री
हिंदी विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय
कलबुरगी, कर्नाटक