72. समकालीन हिन्दी साहित्य और विमर्श – आदिवासी विमर्श – डॉ. एस. विजया
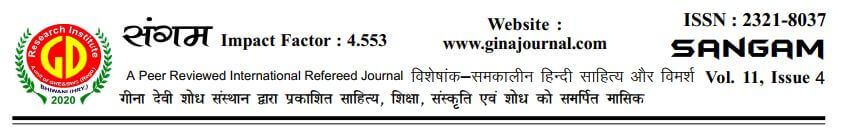 Page No.: 515-526
Page No.: 515-526
समकालीन हिन्दी साहित्य और विमर्श
आदिवासी विमर्श – डॉ. एस. विजया
आदिवासी विमर्श बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में शुरु हुआ अस्मितामूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों के जल जंगल जमीन और जीवन की चिंताएं हैं। माना जाता है कि १९९१ के बाद भारत में शुरु हुए उदारीकरण और मुक्त व्यापार की व्यवस्थाओं ने आदिम काल से संचित आदिवासियों की संपदा के लूट का रास्ता भी खोल दिया। विशाल एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय एवं देशी कंपनियों ने आदिवासी समाज को उनके जल, जंगल और जमीनों से बेदखल कर दिया। इसने आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर विस्थापन को जन्म दिया। बड़ी संख्या में झारखंड, छत्तीसगढ़, दार्जिलिंग आदि इलाकों से लोग बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, कोलकाता आदि में आने को विवश हुए। इन आदिवासी लोगों के पास न धन था, न ही आधुनिक शिक्षा थी। शहरों में ये दिहाड़ी मजदूर या घरेलु नौकर बनने को बाध्य हुए। विशालकाय महानगरों ने इनकी संस्कृति, लोकगीतों और साहित्य को भी निगल लिया। नई पीढ़ी के कुछ आदिवासियों ने शिक्षा हासिल की और अवसरों का लाभ उठाकर सामर्थ्य अर्जित किया। उन्होंने सचेत रूप से अपने समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाना आरंभ किया। उन्होंने संगठन भी बनाए। आदिवासियों ने अपने लिए इतिहास की नए सिरे से तलाश की। उन्होंने अपने नेताओं की पहचान की। अपने लिए नेतृत्व का निर्माण किया। साथ ही समर्थ आदिवासी साहित्य को जन्म दिया। प्रतिरोध अस्मितामूलक साहित्य की मुख्य विशेषता है। आदिवासी विमर्श भी आदिवासी अस्मिता की पहचान, उसके अस्तित्व संबंधी संकटों और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। यह देश के मूल निवासियों के वंशजों के प्रति भेदभाव का विरोधी है।
यह जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा के लिए आदिवासियों के ‘आत्मनिर्णय’ के अधिकार की माँग करता है।
आदिवासी साहित्य की अवधारणा
आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर तीन तरह के मत हैं-
- आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है।
- आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है।
- ‘आदिवासियत’ (आदिवासी दर्शन) के तत्वों वाला साहित्य ही आदिवासी साहित्य है।
पहली अवधारणा गैर-आदिवासी लेखकों की है। परंतु समर्थन में कुछ आदिवासी लेखक भी हैं। जैसे- रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार सिंह, महुआ माजी, बजरंग तिवारी, गणेश देवी आदि गैर-आदिवासी लेखक, और हरिराम मीणा, महादेव टोप्पो, आईवी हांसदा आदि आदिवासी लेखक।
दूसरी अवधारणा उन आदिवासी लेखकों और साहित्यकारों की है जो जन्मना और स्वानुभूति के आधार पर आदिवासियों द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य मानते हैं।
अंतिम और तीसरी अवधारणा उन आदिवासी लेखकों की है, जो ‘आदिवासियत’ के तत्वों का निर्वाह करने वाले साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लेखकों और साहित्यकारों के भारतीय आदिवासी समूह ने 14-15 जून 2014 को रांची (झारखंड) में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस अवधारणा को ठोस रूप में प्रस्तुत किया, जिसे ‘आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा-पत्र’ के तौर पर जाना जा रहा है और अब जो आदिवासी साहित्य विमर्श का केन्द्रीय बिंदु बन गया है।
हिंदी आदिवासी कविताएँ
आदिवासी विमर्श संबंधी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास आदि प्रमुख विधाओं में रचनाएं हुई हैं। इनमें कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। प्रमुख आदिवासी कविता संग्रहों में झारखण्ड की संथाली कवयित्री निर्मला पुतुल की ‘नगाड़े की तरह बजते शब्द’; रामदयाल मुंडा का ‘नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत’ और ‘वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत’ आदि हैं। इसी तरह कुजूर, मोतीलाल और महादेव टोप्पो की कविताएं भी अपने प्रतीक चरित्रों और घटनाओं की कथात्मक संशलिष्टता के कारण विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रही हैं। मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के दौर में आदिवासी कभी पैसे और कभी सरकारी नियमों के बल पर अपनी जमीन से बेदखल होकर पलायन कर रहे हैं। इसके कारण आदिवासी भाषा एवं संस्कृति संकट में पड़ गई है। परंपरागत खेलों से लेकर आदिवासियों की लोक-कला तक विलुप्त होती जा रही है। यह संकट वामन शेलके के यहाँ इस रूप में है-
सच्चा आदिवासी
कटी पतंग की तरह भटक रहा है,
कहते हैं, हमारा देश
इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ रहा है।
मदन कश्यप की कविता “आदिवासी” बाजार के क्रूर चेहरे को सामने लाती है-
ठण्डे लोहे-सा अपना कन्धा ज़रा झुकाओ,
हमें उस पर पाँव रखकर लम्बी छलाँग लगानी है,
मुल्क को आगे ले जाना है।
बाज़ार चहक रहा है
और हमारी बेचैन आकांक्षाओं में साथ-साथ हमारा आयतन भी
बढ़ रहा है,
तुम तो कुछ हटो, रास्ते से हटो।
अनुज लुगुन विस्थापन के भय को स्वर देते हुए लिखते हैं –
बाज़ार भी बहुत बड़ा हो गया है,
मगर कोई अपना सगा दिखाई नहीं देता।
यहाँ से सबका रूख शहर की ओर कर दिया गया है:
कल एक पहाड़ को ट्रक पर जाते हुए देखा,
उससे पहले नदी गयी,
अब खबर फैल रही है कि
मेरा गाँव भी यहाँ से जाने वाला है।
हिंदी आदिवासी गद्य
आदिवासी गद्य साहित्य की शुरुआत बीसवीं सदी के आठवें दशक में हुई। वाल्टर भेंगरा ने झारखण्ड अंचल और वहाँ के जीवन को केंद्र में रखते हुए ‘सुबह की शाम’ उपन्यास लिखा। इसे हिंदी का पहला आदिवासी उपन्यास माना जाता है। पीटर पाल एक्का ने ‘जंगल के गीत’ लिखा। इस उपन्यास में उन्होंने तुंबा टोली गाँव के युवक करमा और उसकी प्रिया करमी के माध्यम से बिरसा मुण्डा के उलगुलान का संदेश पहुंचाया। आदिवासियों द्वारा लिखे गए उपन्यास समकालीन शिल्प और ढाँचों से दूर दिखाई पड़ते हैं। इस कमी की भरपायी गैर आदिवासियों द्वारा लिखे गए आदिवासी उपन्यासों से कुछ हद तक हो गई है। ऐसे उपन्यासों में रमणिका गुप्ता का ‘सीता-मौसी’, कैलाश चंद चौहान का ‘भँवर’, रणेंद्र का ‘ग्लोबल गाँव का देवता’ आदि महत्वपूर्ण हैं। आदिवासियों द्वारा लिखे गए हाल के उपन्यासों में हरिराम मीणा का ‘धूणी तपे तीर’ सर्वाधिक उल्लेखनीय है। रणेंद्र का ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ सिर्फ आग और धातु की खोज करनेवाली और धातु पिघलाकर उसे आकार देनेवाली कारीगर असुर जाति के “जीवन का संतप्त सारांश” है। उपन्यास की शुरुआत इस पीड़ा से होती है- “छाती ठोंक ठोंककर अपने को अत्यन्त सहिष्णु और उदार करनेवाली हिन्दुस्तानी संस्कृति ने असुरों के लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ी थी। वे उनके लिए बस मिथकों में शेष थे। कोई साहित्य नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई अजायबघर नहीं। विनाश की कहानियों के कहीं कोई संकेत्र मात्र भी नहीं’ उपन्यास के अंत तक असुर जनजाति की त्रासदी ‘व्यापक समाज की त्रासदी का प्रारूप बन जाती है।’
साहित्य में आदिवासी
यद्यपि प्रेमचंद के कथा – साहित्य में आदिवासियों को जगह नहीं मिली है और न ही उनका आदिवासियों के जीवन से परिचय था , तथापि उनकी रचनाओं में दो जगहों पर आदिवासियों की चर्चा मिलती है ‘ गोदान ’ उपन्यास में और ‘ सद्गति ’ कहानी में। गोदान में शिकार – प्रसंग में मेहता और मालती की टोली शिकार ढूँढ़ते – ढूँढ़ते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुँच जाती है , जहाँ उनकी मुलाकात वन – कन्या अर्थात् आदिवासी लड़की से होती है। प्रेमचंद ने उस वन – कन्या का चित्रण करते हुए पारंपरिक सौंदर्य चेतना के आलोक में भले ही उसे कुरूप बतलाया हो , पर उसके मांसल शरीर का वर्णन करते हुए मिस्टर मेहता को उसके प्रति आकृष्ट और उसके सेवा – भाव की प्रशंसा करते हुए दिखलाया है। यह वन – कन्या मेहता की पत्नी की कसौटी पर खड़ी उतरती है , अब यह बात अलग है कि दोहरे मानदंडों के साथ जीने वाले मेहता उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारते , वरन् वह मालती को ऊत्तेजित करने और अपने प्रति आकृष्ट करने के साधन भर में तब्दील होकर रह जाती है। मेहता पूरे प्रसंग में आदिवासी लड़की के ‘ अंगों का विलास ’ देखते रहते हैं और मालती से डाँट खाने के बाद आते समय कहते हैं , ‘ अब मुझे आज्ञा दो , बहन ’ । प्रेमचंद पूरे प्रसंग में उस आदिवासी लड़की को नाम भी नहीं देते और उसे ‘ गँवारिन ’ बनाने की कोशिश करते हैं।
इसी प्रकार ‘ सद्गति ’ कहानी आदिवासी संदर्भ में प्रेमचंद के लेखन में आशा की किरण की तरह देखी जा सकती है। इस कहानी में विद्रोही चेतना से लैस एकमात्र पात्र है चिखुरी गोंड़। वह दुखी को पंडित घासीराम के शोषण से बचाने की हर संभव कोशिश करता है , लेकिन धर्मसत्ता के आत्मसातीकरण से उपजे भय के कारण दुखी उससे निकल नहीं पाता और त्रासद मौत का शिकार होता है। उसकी मौत के बाद चमरौने में जाकर वही दलितों को इस अन्याय की खबर देता और आंदोलित करने की कोशिश करता है , ‘ खबरदार , मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है एक गरीब की जान ले ली। पंडितजी होंगे , तो अपने घर के होंगे। ’ इसके बाद पुलिस के भय से कोई भी दलित लाश उठाने नहीं जाता। इस तरह यह कहानी हिंदू धार्मिक संस्कारों से मुक्त एक गोंड़ के माध्यम से ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई की कहानी है , जिसमें दलित और आदिवासी एकता की जरूरत की ओर संकेत भी है।
हरिराम मीणा के ’धूणी तपे तीर‘ में गोविन्द गुरु द्वारा भीलों-मीणों के बीच जागृति फैलाने, संगठित करने और उन्हें अपने हक के लिए बोलना और लड़ना सिखाने तथा बलिदान के लिए तैयार करने की कथा है। यह सन् 1913 ई. में राजस्थान के बाँसवाड़ा अंचल में स्थित मानगढ़ पहाड़ी के आदिवासियों के बलिदान की सच्ची घटना पर आधारित है। आदिवासियों द्वारा सामंतों और औपनिवेशिक शक्तियों की साम्राज्यवादी मानसिकता के विरुद्ध गोविन्द गुरु के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विद्रोह का बिगुल बजाया गया जिसने आगे चलकर औपनिवेशिक दमन की प्रतिक्रिया में हिंसक रूप ले लिया। इस उपन्यास मे लेखक ने आदिवासी-अस्मिता को शोषित-उत्पीड़ित वर्ग और शोषक वर्ग के बीच के वृहत्तर पारंपरिक संघर्ष के रूप में देखा है।
गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासी-विमर्श
स्पष्ट है कि प्रेमचंद भले ही आदिवासी रचनाकार न हों , पर उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिये उस महाजनी सभ्यता के विरुद्ध आवाज उठाई जिनका आदिवासी जीवन एवं समाज में हस्तक्षेप आज भी बदस्तूर जारी है और जो आदिवासी दमन एवं शोषण के मूल में मौजूद है। इन महाजनों की जड़ें आदिवासी क्षेत्रों में न होकर सेमरी एवं बेलारी जैसे गाँवों में हैं और प्रेमचंद इनकी इन्हीं जड़ों पर प्रहार करते हैं। इसीलिए केदार प्रसाद मीना ने सही ही कहा है कि “ प्रेमचंद , रेणु , संजीव और रणेंद्र आदि का साहित्य आदिवासी साहित्य न सही , पर आदिवासियों की समस्याओं पर लिखा गया महत्वपूर्ण साहित्य है। ” वे इस निष्कर्ष के साथ उपस्थित होते हैं कि “उनकी रचनाओं में आदिवासी जीवन की झलक उतनी ही है, जितनी उस जगह पर आदिवासी आबादी है। ” उनका यह भी प्रश्न है कि यदि आज की आदिवासी राजनीति ‘छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ’ में संशोधन के जरिये आदिवासियों की जमीन खरीद – बिक्री के मार्ग को प्रशस्त कर रही है , तो इसमें कोई ‘ प्रेमचंद ’ क्या कर सकते हैं ? इसी प्रकार अगर आदिवासी विमर्श दलित – विमर्श का रास्ता अख्तियार करता है , तो किसी दिन फणीश्वरनाथ ‘ रेणु’ के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ‘मैला आँचल ’ में संथालों को पिटता दिखा कर आनंद प्राप्त किया या उन्हें अपमानित किया है, जो कि सत्य नहीं है।
आदिवासी समस्याओं पर रणेंद्र और संजीव जैसे अच्छे लेखकों की रचनाओं के पात्रों की ऐसी डायरियों , जिनमें आदिवासी समाज का दर्द दर्ज है , को यह उनकी निजी डायरी कह कर इसके बहाने संपूर्ण रचना को खारिज कर रहे हैं। संजीव – रणेंद्र के आदिवासी इलाकों में काम करने वाले पात्र : सुदीप्त और किशन आदि सभी ‘ दिकू ’ नहीं कहे जा सकते। इनकी डायरियाँ महज उनकी निजी डायरियाँ नहीं हैं। ये आदिवासी विस्थापन और उसके खिलाफ संघर्ष के दस्तावेज भी हैं , क्योंकि न तो सरकारें इन्हें दर्ज करती हैं और न विस्थापित करने वाली कंपनियाँ। निरक्षर आदिवासी तो दर्ज कर ही नहीं सकते। ऐसे में इन लेखकों की रचना और इनके पात्रों की डायरियों का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इन लेखकों के साहित्य को ‘दिकू ’साहित्य कहना आदिवासी विमर्श का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ‘जनसत्ता ’ में प्रकाशित आलेख ‘आदिवासी विमर्श के रोड़े ’ के जरिये केदार प्रसाद मीणा आदिवासी – विमर्श को ‘ सहानुभूति – समानुभूति ’ के उस विवाद में उलझने से बचने की सलाह देते हैं जिसने दलित – विमर्श को ‘ साहित्य की राजनीति ’ में ले जाकर उलझा दिया।
आदिवासियों द्वारा आदिवासी – विमर्श
आदिवासी – लेखन हिंदी के अस्मितावादी विमर्शों में सबसे नवीन है। वर्षों से हाशिए पर रखे गये आदिवासी समुदाय को आज साहित्य में जगह मिल रही है और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस दिशा में खुद इस समुदाय के लोगों के द्वारा ही पहल की जा रही है। इस दृष्टि से समकालीन कवि अपनी कविताओं में आदिवासियों के जीवन , उनकी स्थितियों , उनके संघर्षों , उनकी आकांक्षाओं और उनके सपनों को कविता में अभिव्यक्त कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आरंभिक और ज्यादातर आदिवासी साहित्य वाचिक परम्परा का हिस्सा रहा है और इसीलिए यह गीत या कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। यही कारण है कि आदिवासी साहित्य की विधाओं में ’ कविता ’ सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा रही है। इनमें उनके भोगे हुए सत्य के साथ – साथ आदिवासी समाज के सामाजिक – वैयक्तिक जीवन – संघर्ष को अभिव्यक्ति मिली है। इनमें विभिन्न सामाजिक विद्रोह , नारी के जीवन – संघर्ष , विस्थापन , अशिक्षा , अभाव एवं गरीबी और अस्तित्व के प्रश्न को प्रमुखता मिली है।
झारखण्ड की संथाली कवयित्री निर्मला पुतुल ने हिन्दी कविता में अपनी रचना ‘ नगाड़े की तरह बजते शब्द ’ के जरिये अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवायी है। इसी प्रकार ‘नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत’ और ‘वापसी , पुनर्मिलन और अन्य नगीत’ कविता – संग्रह के जरिये रामदयाल मुंडा ने भी पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। उनकी परवर्ती कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के आदिम राग – विराग की जगह राजनीति और समाज की विसंगतियों ने ले ली है। कथन शालवन कगे अंतिम शाल का और विकास का दर्द में उजाड़ बनते झारखंड की व्यथा – कथा और विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। पिछले वर्षों में ग्रेस कुजूर , मोतीलाल , और महादेव टोप्पो की कई कविताएँ भी खूब सराही गयीं। इन कविताओं की हिन्दी पट्टी की कविताओं से भिन्न एवं विशिष्ट है और इस विशिष्ट पहचान का सम्बन्ध जुड़ता है , प्रतीक चरित्रों और घटनाओं के संष्लिष्ट कथात्मक निवेश और प्रतिरोध के आंचलिक रंग से। इसमें जिस यथार्थ का वर्णन हुआ है , वह अमूर्त नहीं है और न ही यह हवा – हवाई है। दरअसल इसके मूल में सहानुभूति की बजाय समानुभूति है और इसीलिए इसमें सतहीपन की बजाय आदिवासी – जीवन से अंतरंगता परिलक्षित होती है, जिसे निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
हिन्दी उपन्यास में आदिवासी विमर्श
हिन्दी जगत पहले – पहल आदिवासी समाज से रूबरू हुआ रेणु के आँचलिक उपन्यास ’ मैला आँचल ‘ में , जब उसने अपने जमीनी हक से बेदखल संथालों को अपने स्वत्व और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखा। यहीं उसका परिचय आदिवासियों की जिजीविषा और जीवटता से भी हुआ और उसने देखा कि प्रशासन की बेरुखी और जुल्म का शिकार होने के बावजूद माँदर एवं डिग्गे की आवाज बंद नहीं हो पाई। लेकिन , एक सच्चे हमदर्द की तरह पीड़ित संथालों के प्रति सहानुभूति के बावजूद यह संघर्ष तार्किक परिणति तक नहीं पहुँच पाता , फलतः उनके जीवन में बदलावों को ला पाने में असमर्थ रहता है। रेणु की समाजवादी यथार्थवादी चेतना और उनका यथार्थवादी आग्रह उन्हें इस समस्या का काल्पनिक एवं आदर्शपरक समाधान देने से रोक देता है। ऐसा नहीं कि ’ मैला आँचल ‘ के बाद आदिवासी जीवन को लेकर रचनाएँ नहीं आयीं , पर उनमें , विशेषकर बस्तर जैसे अंचलों को लेकर लिखी गयी रचनाओं में लेखक की दिलचस्पी स्वच्छंद प्रेम की घोटुल – प्रथा जैसे अतिरेकवादी तत्वों को लेकर कहीं ज्यादा थी। आगे चलकर महाश्वेता देवी के उपन्यास ‘हजार चैरासी की माँ ’ एक सशक्त एवं प्रभावी हस्तक्षेप के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी और नक्सलवाद को लेकर एक नए नजरिए से हिन्दी जगत को रूबरू करवाया। उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि नक्सली हिंसा ऐतिहासिक परिस्थितियों और एक लम्बे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय की उपज है। अपने परवर्ती उपन्यासों में भी महाश्वेता देवी ने आदिवासियों की विद्रोही चेतना को अभिव्यक्ति देते हुए हिन्दी के पाठकों को बिरसा मुण्डा जैसे महानायक से परिचित करवाया। लेकिन , औपन्यासिक धरातल पर आदिवासी विमर्श की परम्परा 1980 के दशक में शुरू होते देखा जा सकता है। हेराल्ड एस . टोप्पनो के अधूरे ( प्रकाशित ) उपन्यास को पढ़ते हुए एक विस्फोटक संभावना से भेंट होती है। आठवें दशक में वाल्टर भेंगरा ने झारखण्ड अंचल और वहाँ के जीवन को केंद्र में रखते हुए ‘ सुबह की शाम ’ उपन्यास लिखा जो आदिवासियों के द्वारा लिखा गया पहला हिन्दी उपन्यास है। पिछले दशक में उनके तीन उपन्यास : तलाश , गैंग लीडर और कच्ची कली प्रकाशित हुए। लेकिन , पिछले दिनों पीटर पाल एक्का के उपन्यास जंगल के गीत की सबसे अधिक चर्चा हुई जिसके जरिये एक्का ने बिरसा मुण्डा के उलगुलान के संदेश को तुंबा टोली गाँव के युवक करमा और उसकी प्रिया करमी के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की। इससे पहले भी उनका एक उपन्यास मौन घाटी के नाम से प्रकाशित हो चुका है। झारखंड के इन आदिवासी कथाकारों की समस्या यह है कि वे आधुनिक लेखन के सामयिक रूझानों और शिल्प – साँचों से अपरिचित प्रतीत होते हैं।
लेकिन, मुख्यधारा इसकी कुछ हदतक भरपाई करती हुई आती है। इस दृष्टि से रमणिका गुप्ता के उपन्यास ‘सीता – मौसी ’और कैलाश चंद चैहान के उपन्यास ‘भँवर’ के साथ – साथ संजीव एवं रणेंद्र के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के बड़े आंदोलन से जुड़े होने के कारण हरिराम मीना के उपन्यास ‘धूणी तपे तीर ’ को भी काफी चर्चा मिली है जिसे बिहारी सम्मान से नवाजा गया।
उपसंहार
स्पष्ट है कि आदिवासी समाज सदियों से जातिगत भेदों , वर्ण व्यवस्था , विदेशी आक्रमणों , अंग्रजों और वर्तमान में सभ्य कहे जाने वाले समाज ( तथाकथित मुख्यधारा के लोग ) द्वारा दूर – दराज जंगलों और पहाड़ों में खदेड़ा गया है। अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण उन्हें सताया गया है। अक्षरज्ञान न होने के कारण यह समाज सदियों से मुख्यधारा से कटा रहा , दूरी बनाता रहा। उनकी लोककला और उनका साहित्य सदियों से मौखिक रूप में रहा हैं और इसका कारण रहा उनकी भाषा के अनुरूप लिपि का विकसित न हो पाना। यही कारण साहित्य जगत में आदिवासी रचनाकार और उनका साहित्य गैर – आदिवासी साहित्य की तुलना में कम मिलता है। आज भले ही आदिवासियों की रचनाओं में एक प्रकार की अनगढ़ता एवं खुरदरापन दिखे और कलात्मक बारीकियों के आलोक में उनका मूल्यांकन पाठकों एवं आलोचकों को निराश करता हो पर इसका महत्व इस बात में है कि इसने मुख्यधारा के द्वारा उपेक्षित एवं तिरस्कृत आदिवासी समाज एवं उनके जीवन से व्यापक समाज को परिचित करवाने की कोशिश की।
धन्यवाद
डॉ. एस. विजया
सहायक प्रोफेसर
एम जैन कॉलेज, चेन्नई